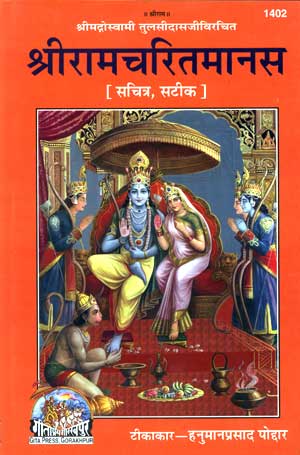|
रामायण >> श्रीरामचरितमानस अर्थात तुलसी रामायण (उत्तरकाण्ड) श्रीरामचरितमानस अर्थात तुलसी रामायण (उत्तरकाण्ड)गोस्वामी तुलसीदास
|
|
||||||
भारत की सर्वाधिक प्रचलित रामायण। सप्तम सोपान उत्तरकाण्ड
दो.-मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह।
हरि जन द्विज देखें जरउँ करउँ बिष्नु कर द्रोह।।105क।।
हरि जन द्विज देखें जरउँ करउँ बिष्नु कर द्रोह।।105क।।
मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश
श्रीहरिके भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णुभगवान् से द्रोह
करता था।।105(क)।।
सो.-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम।।
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति की भावई।।105ख।।
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति की भावई।।105ख।।
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भलीभाँति
समझाते, पर [मैं कुछ भी नहीं समझता] उलट मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता।
दम्भीको कभी नीति अच्छी लगती है?।।105(ख)।।
चौ.-एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई।।
सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई।।1।।
सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई।।1।।
एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से
[परमार्थ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र! शिवजीकी सेवा का फल यही है कि
श्रीरामजीके चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो।।1।।
रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर पावँर कै केतिक बाता।।
जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी।।2।।
जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी।।2।।
हे तात! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजी को भजते हैं, [फिर]
नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है? ब्रह्माजी और शिव जी जिनके चरणों के
प्रेमी हैं, अरे अभागे! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है?।।2।।
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ।।
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ।।3।।
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ।।3।।
गुरुजीने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षिराज!
मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से
साँप।।3।।
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करउँ दिनु
राती।।
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा।।4।।
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा।।4।।
अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे
द्रोह करता। गुरुजी अत्यन्त दयालु थे। उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता।
[मेरे द्रोह करने पर भी] वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी शिक्षा देते
थे।।4।।
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहिं हति ताहि नसावा।।
धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई।।5।।
धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई।।5।।
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर
उसी का नाश करता है। हे भाई! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआँ मेघकी पदवी
पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है।।5।।
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई।।
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई।।6।।
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई।।6।।
धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब [राह चलने
वालों] के लातों की मार सहती है पर जब पवन उसे उड़ाता (ऊँचा उठाता) है, तो
सबसे पहले वह उसी (पवन) को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों
(मुकुटों) पर पड़ती है।।6।।
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिंअधम कर
संगा।।
कबि कोबिद गावहिं असि नीति। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती।।7।।
कबि कोबिद गावहिं असि नीति। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती।।7।।
हे पक्षिराज गरुड़जी! सुनिये, बात समझकर बुद्धिमान् लोग अधम
(नीच) का संग नहीं करते। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न
कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही।।7।।
उदासीन नित रहिअ गोसाईं। खल परिहरिअ स्वान की नाईं।।
मैं खल हृदयँ कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई।।8।।
मैं खल हृदयँ कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई।।8।।
हे गोसाईं! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्ट को
कुत्ते की तरह दूरसे ही त्याग देना चाहिये। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और
कुटिलता भरी थी। [इसलिये यद्यपि] गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह
सुहाती न थी।।8।।
दो.-एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नाम।
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम।।106क।।
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम।।106क।।
एक दिन मैं शिव जी के मन्दिर में शिवनाम जप कर रहा था। उसी
समय गुरुजी वहाँ आये, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं
किया।।106(क)।।
सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस।।
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस।।106ख।।
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस।।106ख।।
गुरुजी दयालु थे, [मेरा दोष देखकर भी] उन्होंने कुछ नहीं कहा;
उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा
पाप है; अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके ।।106(ख)।।
चौ.-मंदिर माझ भई नभ बानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी।।
जद्यपि तव गुर कें नहिं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा।।1।।
जद्यपि तव गुर कें नहिं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा।।1।।
मन्दिर में आकाश वाणी हुई कि अरे हतभाग्य! मूर्ख! अभिमानी!
यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्त के हैं और
उन्हें [पूर्ण तथा] यथार्थ ज्ञान हैं, ।।1।।
तदपि साप सठ दैहउँ तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोही।।
जौं नहिं दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा।।2।।
जौं नहिं दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा।।2।।
तो भी हे मूर्ख! तुझको मैं शाप दूँगा। [क्योंकि] नीति का
विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट! यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा
वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाय।।2।।
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं।।
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा।।3।।
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा।।3।।
जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों
तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर (वहाँ से निकल कर) वे तिर्यग्
(पशु, पक्षी आदि) योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक
दुःख पाते रहते हैं।।3।।
बैठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मति ब्यापी।।
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई।।4।।
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई।।4।।
अरे पापी! तू गुरु के सामने अजगर की भाँति बैठा रहा! रे दुष्ट
! तेरी बुद्धि पाप से ढक गयी है, [अतः] तू सर्प हो जा। और, अरे अधम से भी
अधम ! इस अद्योगति (सर्प की नीची योनि) को पाकर किसे बड़े भारी पेड़ के
खोखले में जाकर रह।।4।।
दो.-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप।
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप।।107क।।
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप।।107क।।
शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया। मुझे काँपता
हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ।।107(क)।।
करिं दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि।।
बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि।।107ख।।
बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि।।107ख।।
प्रेम सहित दण्डवत् करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजी के सामने हाथ
जोड़कर मेरी भयंकर गति (दण्ड) का विचार कर गद्गद वाणी से विनती करने
लगे।।107(ख)।।
छं.-नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म
वेदस्वरुपं।।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं।।1।।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं।।1।।
हे मोक्षस्वरुप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरुप, ईशान
दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
निजस्वरुप में स्थित (अर्थात् मायादिरहित) [मायिक] गुणोंसे रहित, भेदरहित,
इच्छारहित, चेतन, आकाशरुप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिम्बर
[अथवा आकाशको भी आच्छादित करनेवाले] आपको मैं भजता हूँ।।1।।
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं।।
करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं।।2।।
करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं।।2।।
निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय (तीनों गुणों से अतीत), वाणी,
ज्ञान और इन्द्रियों से परे, कैलासपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु,
गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ।।2।।
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री
शरीरं।।
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा।।3।।
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा।।3।।
जो हिमालय के समान गौर वर्ण तथा गम्भीर हैं, जिसके शरीर में
करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुन्दर नदी गंगाजी
विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चन्द्रमा और गले में सर्प सुशोभित
हैं।।3।।
चलत्कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठं
दयालं।।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।।4।।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।।4।।
जिनके कानों के कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भृकुटी और विशाल
नेत्र हैं; जो प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और दयालु हैं; सिंहचर्म का वस्त्र धारण
किये और मुण्डमाला पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ [कल्याण करनेवाले]
श्रीशंकरजी को मैं भजता हूँ।।4।।
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं
भानुकोटिप्रकाशं।।
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं।।5।।
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं।।5।।
प्रचण्ड (रुद्ररूप), श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड,
अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकार के शूलों
(दुःखों) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्रिशूल धारण किये, भाव (प्रेम) के
द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानी के पति श्रीशंकरजी को मैं भजता हूँ।।5।।
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी।।
चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।।6।।
चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।।6।।
कलाओं से परे, कल्याण, स्वरुप, कल्प का अन्त (प्रलय) करने
वाले, सज्जनों को सदा आनन्द देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानन्दघन,
मोह को हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेव के शत्रु हे प्रभो! प्रसन्न
हूजिये प्रसन्न हूजिये।।6।।
न यावद् उमानाथ पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नराणां।।
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।।7।।
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।।7।।
जबतक पार्वती के पति आपके चरणकमलों को मनुष्य नहीं भजते, तबतक
उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापों का
नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर (हृदय में) निवास करनेवाले प्रभो!
प्रसन्न हूजिये।।7।।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु
तुभ्यं।।
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो।।8।।
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो।।8।।
मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शम्भो! मैं तो
सदा-सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो! बुढ़ापा तथा जन्म [मृत्यु]
के दुःख समूहों से जलते हुए मुझ दुःखीकी दुःखसे रक्षा करिये। हे ईश्वर! हे
शम्भो! मैं नमस्कार करता हूँ।।8।।
श्लोक-रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये।।
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।।9।।
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।।9।।
भगवान् रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि
(प्रसन्नता) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक
पढ़ते हैं, उनपर भगवान् शम्भु प्रसन्न हो जाते हैं।।9।।
दो.-सुनि बिनती सर्बग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु।
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मागु।।108क।।
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मागु।।108क।।
सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब
मन्दिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ! वर माँगो।।108(क)।।
जौं प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु।
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु।।108ख।।
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु।।108ख।।
[ब्राह्मणने कहा-] हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे
नाथ! यदि इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर
दूसरा वर दीजिये।।108(ख)।।
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान।।108ग।।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान।।108ग।।
हे प्रभो! यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरन्तर भूला
फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान्! उसपर क्रोध न कीजिये।।108(ग)।।
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल।
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल।।108घ।।
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल।।108घ।।
हे दीनों पर दया करने वाले (कल्याणकारी) शंकर! अब इसपर कृपालु
होइये (कृपा कीजिये), जिससे हे नाथ! थोड़े ही समय में इसपर शापके बाद
अनुग्रह (शाप से मुक्ति) हो जाय।।108(घ)।।
चौ.-एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना।।
बिप्रगिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभबानी।।
बिप्रगिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभबानी।।
हे कृपा के निधान! अब वही कीजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो।
दूसरेके हितसे सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाश वाणी हुई-एवमस्तु
(ऐसा ही हो)।।1।।
जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा। मैं पुनि दीन्हि कोप करि
सापा।।
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर कृपा बिसेषी।।2।।
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर कृपा बिसेषी।।2।।
यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके
शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूँगा।।2।।
छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी।।
मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि।।3।।
मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि।।3।।
हे द्विज! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे
ही प्रिय हैं जैसे खरारि श्रीरामचन्द्रजी । हे द्विज! मेरा शाप व्यर्थ नहीं
जायगा यह हजार जन्म अवश्य पावेगा।।3।।
जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वल्पउ नहिं ब्यपिहि सोई।।
कवनेउ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना।।4।।
कवनेउ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना।।4।।
परन्तु जन्मने में और मरने में जो दुःसह दुःख होता है, इसको
वह दुःख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे
शूद्र! मेरा प्रामाणिक (सत्य) बचन सुन ।।4।।
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनि तैं मम सेवाँ मन दयऊ।।
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरें।।5।।
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरें।।5।।
[प्रथम जो] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजी की पुरी में हुआ। फिर तूने
मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदय में
रामभक्ति होगी।।5।।
सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई।।
अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना।।6।।
अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना।।6।।
हे भाई! अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजोंकी सेवा ही भगवान् को
प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को
अनन्त श्रीभगवान् ही के समान जानना।।6।।
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरि चक्र कराला।।
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। बिप्रद्रोह पावक सो जरई।।7।।
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। बिप्रद्रोह पावक सो जरई।।7।।
इन्द्र के वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, कालके दण्ड और
श्रीहरिके विकराल चक्रके मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोहीरूपी
अग्नि से भस्म हो जाता है।।7।।
अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहँ जग दुर्लभ कछु
नाहीं।।
औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी।।8।।
औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी।।8।।
ऐसा विवेक मन में रखना। फिर तुम्हारे लिये जगत् में कुछ भी
दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति
होगी (अर्थात् तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं बिना रोक-टोक के जा सकोगे।।8।।
दो.-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि ।।
मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि।।109क।।
मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि।।109क।।
[आकाशवाणीके द्वारा] शिवजी के वचन गुरुजी सुनकर हर्षित होकर
ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर
अपने घर गये।।109(क)।।
प्रेरित काल बिंधि गिरि जाइ भयउँ मैं ब्याल।
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल।।109ख।।
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल।।109ख।।
काल की प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ
काल बीतने पर बिना ही परिश्रम (कष्ट) के मैंने वह शरीर त्याग
दिया।।109(ख)।।
जोइ तनु धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान।।
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान।।109ग।।
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान।।109ग।।
हे हरिवाहन! मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम
वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है
और नया पहिन लेता है।।109(ग)।
सिवँ राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा क्लेस।
एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु ग्यान न गयउ खगेस।।109घ।।
एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु ग्यान न गयउ खगेस।।109घ।।
शिवजीने वेदकी मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं
पाया। इस प्रकार हे पक्षिराज! मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान
नहीं गया।।109(घ)।।
चौ.-त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन
अनुसरऊँ।।
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ।।1।।
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ।।1।।
तिर्यक् योनि (पशु-पक्षी) देवता या मनुष्य का, जो भी शरीर
धारण करता, वहाँ-वहाँ (उस-उस शरीरमें) मैं श्रीरामजी का भजन जारी रखता। [इस
प्रकार मैं सुखी हो गया ] परन्तु एक शूल मुझे बना रहा। गुरुजी का कोमल,
सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता (अर्थात् मैंने ऐसा कोमल स्वभाव दयालु
गुरुका अपमान किया, यह दुःख मुझे सदा बना रहा)।1।।
चरम देह द्विज कै मैं पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई।।
खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला।।2।।
खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला।।2।।
मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद
देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ (ब्राह्मण-शरीरमें) भी बालकों
में मिलकर खेलता तो श्रीरघुनाथजीकी ही सब लीलाएँ किया करता।।2।।
प्रौढ़ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं
भावा।।
मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी।।3।।
मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी।।3।।
सयाना होनेपर पिता जी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और
विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएँ भाग
गयीं। केवल श्रीरामजी के चरणों में लव लग गयी।।3।।
कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी।।
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई।।4।।
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई।।4।।
हे गरुड़जी! कहिये, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर
गदहीकी सेवा करेगा? प्रेममें मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता।
पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये।।4।।
भए कालबस जब पितु माता। मैं बन गयउँ भजन जनत्राता।।
जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ।।5।।
जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ।।5।।
जब पिता-माता कालवाश हो गये (मर गये), तब मैं भक्तों की रक्षा
करनेवाले श्रीरामजीका भजन करने के लिये वन में चलता गया। वन में जहाँ-जहाँ
मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता।।5।।
बूझउँ तिन्हहि राम गुन गाहा। कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा।।
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुबादा। अब्याहत गति संभु प्रसादा।।6।।
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुबादा। अब्याहत गति संभु प्रसादा।।6।।
उनसे मैं श्रीरामजीके गुणों की कथाएँ पूछता। वे कहते और मैं
हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता
फिरता। शिवजी की कृपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी (अर्थात् मैं जहाँ
चाहता वहीं जा सकता था)।।6।।
छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी।
राम चरन बारिज जब देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं।।7।।
राम चरन बारिज जब देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं।।7।।
मेरी तीनों प्रकार की (पुत्रकी, धनकी और मानकी) गहरी प्रबल
वासनाएँ छूट गयीं। और हृदय में एक ही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब
श्रीरामजीके चरणकमलों के दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ।।7।।
जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर सर्ब भूतमय अहई।।
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई।।8।।
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई।।8।।
जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है।
यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही
थी।।8।।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book